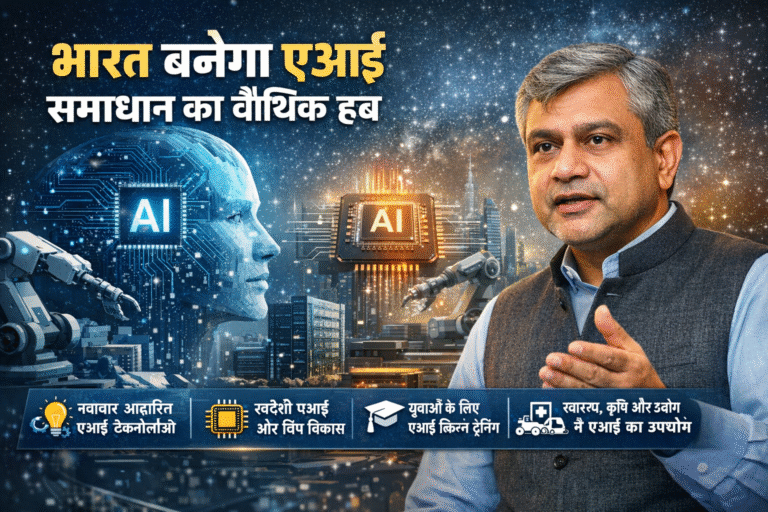अलंकार जैन
सदस्य बाल कल्याण समिति जिला भोपाल
9174775777
देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विरोध दिखाई दे रहा है, वह केवल एक शैक्षणिक निर्णय के प्रति असहमति नहीं है। यह विरोध दरअसल उस गहरी सामाजिक बेचैनी की अभिव्यक्ति है, जो लंबे समय से देश की नीतियों, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था, के भीतर पल रही है। यह स्थिति हमें एक मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए विवश करती है—क्या ऐसे विवादों की जड़ केवल नीतियों में है, या फिर उस संवैधानिक ढाँचे में भी है जिसने समाज को अनेक वर्गों और पहचानों में बाँट दिया?
भारतीय संविधान समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। परंतु व्यवहारिक स्तर पर नागरिकों को एक समान इकाई के रूप में देखने के बजाय, उन्हें जाति, वर्ग और श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। यही विभाजन समय के साथ सामाजिक पहचान बन गया और नीतियों का केंद्र भी।
शिक्षा जैसे क्षेत्र में, जहाँ योग्यता और परिश्रम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वहाँ भी वर्ग-आधारित नियम, कट-ऑफ और अवसरों की अलग-अलग परिभाषाएँ बन गईं। परिणामस्वरूप जब भी यूजीसी जैसे संस्थान कोई नया नियम लाते हैं, तो उसका मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर होता है कि किस वर्ग को कितना लाभ या हानि हुई।
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था। परंतु जो व्यवस्थाएँ अस्थायी सुधार के लिए बनाई गई थीं, यदि वे स्थायी सामाजिक पहचान बन जाएँ, तो समानता का मूल लक्ष्य पीछे छूटने लगता है। आज असंतोष इसी कारण गहराता जा रहा है।
इसी असंतोष की चरम अभिव्यक्ति के रूप में समाज में एक व्यावहारिक लेकिन विवादास्पद सुझाव भी सुनाई देने लगा है—कि जब तक यूजीसी नियम और वर्ग-आधारित व्यवस्थाएँ लागू हैं, तब तक सवर्ण वर्ग के लिए अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा अन्य वर्गों के लिए अलग शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएँ, ताकि प्रवेश, आरक्षण और अवसरों को लेकर होने वाला निरंतर संघर्ष समाप्त हो सके।
यह सुझाव न तो आदर्श है और न ही राष्ट्रीय एकता के दीर्घकालिक हित में। परंतु इसे केवल कट्टर या विभाजनकारी कहकर खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। दरअसल यह प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि वर्तमान व्यवस्था से असंतोष किस हद तक पहुँच चुका है। जब समाज अलगाव को समाधान के रूप में देखने लगे, तो समझना चाहिए कि समस्या केवल नियमों में नहीं, बल्कि उस मूल ढाँचे में है जो लगातार टकराव पैदा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के निर्णय में स्पष्ट कहा था कि आरक्षण अपवाद होना चाहिए, सामान्य नियम नहीं। यदि अपवाद ही स्थायी व्यवस्था बन जाए, तो असंतुलन और असंतोष स्वाभाविक है। शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) तभी सार्थक हो सकता है, जब शिक्षा का वातावरण शांत, समान और प्रतिस्पर्धात्मक हो—न कि वर्गीय तनाव से ग्रस्त।
संविधान कोई जड़ ग्रंथ नहीं है। वह समय-समय पर आत्ममंथन और सुधार की अपेक्षा करता है। यदि किसी व्यवस्था से निरंतर विरोध, अस्थिरता और सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर प्रश्न उठाना संविधान-विरोध नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा का प्रयास है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता की समानता पर गंभीरता से विचार करें। जब तक हर नीति को वर्गीय चश्मे से देखा जाएगा, तब तक यूजीसी जैसे संस्थानों के नियम सुधार नहीं, संघर्ष का कारण ही बनेंगे।
सच्ची समानता और राष्ट्रीय एकता तभी संभव है, जब हम स्वयं को पहले और अंततः समान नागरिक मानने का साहस करें—न कि स्थायी वर्गों में बँटी हुई पहचान के रूप में।